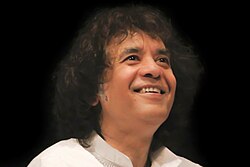More actions
साँचा:Infobox Instrument तबला[nb १] भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक तालवाद्य है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों में बहुत प्रचलित है।[१] यह लकड़ी के दो ऊर्ध्वमुखी, बेलनाकार, चमड़ा मढ़े मुँह वाले हिस्सों के रूप में होता है, जिन्हें रख कर बजाये जाने की परंपरा के अनुसार "दायाँ" और "बायाँ" कहते हैं। यह तालवाद्य हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में काफी महत्वपूर्ण है और अठारहवीं सदी के बाद से इसका प्रयोग शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन-वादन में लगभग अनिवार्य रूप से हो रहा है। इसके अतिरिक्त सुगम संगीत और हिंदी सिनेमा में भी इसका प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। यह बाजा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, और श्री लंका में प्रचलित है।[२] पहले यह गायन-वादन-नृत्य इत्यादि में ताल देने के लिए सहयोगी वाद्य के रूप में ही बजाय जाता था, परन्तु बाद में कई तबला वादकों ने इसे एकल वादन का माध्यम बनाया और काफी प्रसिद्धि भी अर्जित की।
नाम तबला की उत्पत्ति अरबी-फ़ारसी मूल के शब्द "तब्ल" से बतायी जाती है।[३] हालाँकि, इस वाद्य की वास्तविक उत्पत्ति विवादित है - जहाँ कुछ विद्वान् इसे एक प्राचीन भारतीय परम्परा में ही उर्ध्वक आलिंग्यक वाद्यों[४] का विकसित रूप मानते हैं वहीं कुछ इसकी उत्पत्ति बाद में पखावज से निर्मित मानते हैं और कुछ लोग इसकी उत्पत्ति का स्थान पच्छिमी एशिया भी बताते हैं।[५]
उत्पत्ति
तबले का इतिहास सटीक तौर पर नामालूम है और इसकी उत्पत्ति के बारे में कई उपस्थापनायें मौजूद हैं।[५][६] इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में वर्णित विचारों को दो समूहों में बाँटा जा सकता है:[५]
तुर्क-अरब उत्पत्ति
औपनिवेशिक शासन के दौरान इस परिकल्पना को काफी बलपूर्वक पुरःस्थापित किया गया कि तबले की मूल उत्पत्ति मुस्लिम सेनाओं के साथ चलने वाले जोड़े ड्रम से हुई है; इस स्थापना का मूल अरबी के "तब्ल" शब्द पर आधारित है जिसका अर्थ "ड्रम (ताल वाद्य)" होता है। बाबर द्वारा सेना के साथ ऐसे ड्रम लेकर चलने को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, हालाँकि तुर्क सेनाओं के साथ चलने वाले ये वाद्ययंत्र तबले से कोई समानता नहीं रखते बल्कि "नक्कारा" (भीषण आवाज़ पैदा करने वाले) से समानता रखते हैं।[५]
दूसरी स्थापना के मुताबिक़, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अमीर ख़ुसरो ने "आवाज़ बाजा" (बीच में पतला तालवाद्य) को काट कर तबले का रूप देने की बात कही जाती है। हालाँकि, यह भी संभव नहीं लगता क्योंकि उस समय के कोई भी चित्र इस तरह के किसी वाद्य यंत्र का निरूपण नहीं करते। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी अपने विवरणों में ऐसे किसी वाद्ययंत्र का उल्लेख नहीं किया है। उदाहरण के लिए, अबुल फैजी ने आईन-ए-अकबरी में तत्कालीन वाद्ययंत्रों की लंबी सूची गिनाई है, लेकिन इसमें तबले का ज़िक्र नहीं है।[५]
एक अन्य तीसरे मतानुसार दिल्ली के ख़यात गायक सदारंग के शिष्य और प्रसिद्ध पखावज वादक रहमान खान के पुत्र, अमीर खुसरो (द्वितीय) ने 1738 ई॰ में पखावज से तबले का आविष्कार किया।[७] इससे पहले ख़याल गायन में भी पखावज से संगत की जाती थी। इस सिद्धांत में सत्यता संभावित है क्योंकि उस समय की लघु कलाकृतियों (मिनियेचर पेंटिंग) में तबले से मिलते-जुलते वाद्ययंत्र के प्रमाण मिलते हैं। हालाँकि, इससे यह प्रतीत होता है की इस वाद्ययंत्र की उत्पत्ति भारतीय उपमहादीप के मुस्लिम समुदायों में दिल्ली के आसपास हुई न कि यह अरब देशों से आयातित वाद्ययंत्र है।[५][८] नील सोर्रेल और पंडित राम नारायण जैसे संगीतविद पखावज काट कर तबला बनाये जाने की इस किम्वदंती में बहुत सत्यता नहीं देखते।[९]
भारतीय उत्पत्ति
भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानने वाले तबले का मूल भारत में मानते हैं और यह कहते हैं कि मुस्लिम काल में इसने मात्र अरबी नाम ग्रहण कर लिया।[६] भारतीय नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के द्वारा उर्ध्वक आलिंग्यक वाद्यों के वर्णन की बात कही जाती है।[४] ऐसे ही, हाथ में लेकर बजाये जाने वाले "पुष्कर" नामक तालवाद्यों से तबले की उत्पत्ति बतायी जाती है। "पुष्कर" वाद्य के प्रमाण छठवीं-सातवीं सदी के मंदिर उत्कीर्णनों में, ख़ासतौर पर मुक्तेश्वर और भुवनेश्वर मंदिरों में, प्राप्त होते हैं।[६][१०][१२] इन कलाकृतियों में वादक कलाकार दो या तीन अलग-अलग रखे तालवाद्यों को सामने रख कर बैठे दिखाए गए हैं और उनके हाथों और उँगलियों के निरूपण से वे इन्हें बजाते हुए प्रतीत होते हैं।[१०] हालाँकि, इन निरूपणों से यह नहीं पता चलता कि ये वाद्ययंत्र उन्हीं पदार्थों से निर्मित हैं और चर्मवाद्य ही हैं, जैसा की आधुनिक समय का तबला होता है।[१०]
तबला आज जिन पदार्थों से और जिस रूप में बनाया जाता है, ऐसे वाद्ययंत्रों के निर्माण के लिखित प्रमाण संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध हैं। "तबला"-जैसे वाद्ययंत्र के निर्माण सम्बन्धी सबसे पुरानी जानकारी संस्कृत नाट्य शास्त्र में मिलती है।[१०] इन तालवाद्यों को बजाने से सम्बंधित विवरण भी नाट्यशास्त्र में मिलती है। वहीं, दक्षिण भारतीय ग्रंथ, उदाहरणार्थ, शिलप्पदिकारम, जिसकी रचना प्रथम शताब्दी ईसवी मानी जाती है, लगभग तीस ताल वाद्यों का विवरण देता है जिनमें कुछ रस्सियों द्वारा कसे जाने वाले और अन्य शामिल हैं, लेकिन इसमें "तबला" नामक किसी वाद्य का विवरण नहीं है।[१३]
इतिहास

ताल और तालवाद्यों का वर्णन वैदिक साहित्य से ही मिलना शुरू हो जाता है।[१५][१६] दो या तीन अंगों वाला, डोरियों के सहारे लटका कर, हाथों से बजाये जाने वाले वाद्य यंत्र पुष्कर (अथवा "पुष्कल") के प्रमाण पाँचवीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं जो मृदंग के साथ अन्य तालवाद्यों में गिने जाते थे, हालाँकि, तब इन्हें तबला नहीं कहा जाता था।[१७] पांचवीं सदी से पूर्व की अजंता गुफाओं के भित्ति-चित्र जमीन पर रख कर बजाये जाने वाले ऊर्ध्वमुखी ड्रमों का निरूपण करते हैं।[१८] बैठ का ताल वाद्य बजाते हुए कलाकारों का ऐसा ही निरूपण एलोरा की प्रस्तर मूर्तियों में मिलता है,[१९] तथा अन्य स्थलों से भी।[२०]
पहली सदी के चीनी-तिब्बती यात्रियों द्वारा भी भारत में छोटे आकार के ऊर्ध्वमुखी ड्रमों का प्रचलन होने का विवरण प्राप्त होता है (पुष्कर को तिब्बती साहित्य में "जोंग्पा" कहा गया है)।[२१] जैन और बौद्ध ग्रंथों, जैसे समवायसूत्र, ललितविस्तार और सूत्रालंकार इत्यादि में भी पुष्कर नामक इस तालवाद्य के विवरण मिलते हैं।[२२]
कई हिन्दू और जैन मंदिर, जैसे की राजस्थान के जयपुर स्थित एकलिंगजी मंदिर, तबले जैसे आकार के वाद्य बजाते हुए व्यक्ति का प्रस्तर मूर्तियों में निरूपण करते हैं। दक्षिण में यादव शासन के समय (1210 से 1247) में भी आईएस तरह के छोटे तालवाद्यों का प्रमाण मिलता है जब सारंगदेव संगीत रत्नाकर की रचना कर रहे थे। हालिया बिंबशास्त्रीय दावे जिनमें तबले को 1799 के आसपास का माना गया है[२३] अब महत्वहीन हो चुकी हैं और भाजे गुफाओं से प्राप्त चित्र प्राचीन भारत में इस तरह के वाद्य का प्रयोग प्रमाणित करते हैं। जमीन पर रख कर बजाये जाने वाले ऊर्ध्वमुखी वाद्यों के प्रमाण कई हिन्दू मंदिरों से प्राप्त हुए हैं जो 500 ईपू के आसपास तक के समय के हैं।[२४] दक्षिण भारत में इसतरह के वाद्यों के मौजूद होने के प्रमाण के रूप में होयसलेश्वर मंदिर, कर्नाटकम का उदाहरण लिया जा सकता है जिसमें एक नक्काशी में नृत्य समारोह में एक स्त्री तबले जैसे वाद्य बजाती दिखाई गयी है।[२५]
तबला, बजाने की कला के आधार पर मृदंग और पखावज से अलग है। इसमें हाथ की उंगलियों की कलात्मक गति का महत्व अधिक है। वहीं, पखावज और मृदंग पंजों की गति से बजाये जाते हैं क्योंकि इनपर आघात क्षैतिज रूप से किया जाता है और इस प्रकार इनके बोलों में जटिलता उतनी नहीं जितनी तबले में पाई जाती है।[२६] अतः ध्वनिशास्त्रीय और वादन कला आधारित अध्ययनों में तबले की समानता तीनों वाद्यों के साथ स्थापित की जा सकती है; पखावज की तरह का "दायाँ", नक्कारे की तरह आकार वाला "बायाँ", ढोलक की तरह गमक वाला प्रयोग, तीनों प्राप्त होते हैं।[२७]
अंग
"तबला" के दो अंग होते हैं, अर्थात इसमें दो ड्रम होते हैं जिनका आकार और आकृति एक दूसरे से कुछ भिन्नता लिए होती है।[२][२८][२९] तकनीकी तौर पर, एक सीधे हाथ वाले वादक द्वारा, दाहिने हाथ (कुशल हाथ) से बजाय जाने वाला अंग ही तबला कहलाता है। आम भाषा में इसे दायाँ या दाहिना कहते हैं। यह लगभग 15 सेंटीमीटर (~6 इंच) व्यास वाला और 25 सेंटीमीटर (~10 इंच) ऊँचाई वाला होता है।
बायें वाले हिस्से को क्षेत्र अनुसार डग्गा, डुग्गी अथवा धामा भी कहते हैं। पुराने प्राप्त चित्रों में दाहिने और बायें अंग का आकार लगभग समान पाया गया है और कभी कभी बायें का आकर छोटा भी।[४] हालाँकि, अब बायाँ का आकार तबले की तुलना में काफी बड़ा होता है। दाहिना या तबला बहुधा लकड़ी का बना होता है जबकि बायाँ मिट्टी (पके बर्तन के रूप में जिस पर चमड़ा मढ़ा जाय) का भी होता है अथवा दोनों ही पीतल या फूल (मिश्र-धातु) के भी बने हो सकते हैं। बायाँ, चौड़े मुँह वाला, चमड़े मढ़ा ड्रम होता है जिसका आकार लगभग 20 सेंटीमीटर (~8 इंच) व्यास वाला और 25 सेंटीमीटर (~10 इंच) ऊँचाई वाला होता है।
दाहिने में डोरियों के बीच (जो अक्सर चमड़े की ही होती हैं) लकड़ी के छोटे आड़े बेलन बेलन लगे होते हैं, जिनपर हथौड़ी से चोट कर डोरियों के कसाव को बदला जा सकता है। इस क्रिया को सुर मिलाना कहते हैं। गायन-वादन के दौरान राग के मुख्य स्वर "सा" के साथ तबले की ध्वनि की तीक्ष्णता का मिलान किया जाता है, जिसे तबले को "षडज" पर मिलाना कहते हैं।[२][९] सितार के साथ, चूँकि तार वाद्य और ऊँची तीक्ष्णता का वाद्य है, तबले को "पंचम" पर भी मिलाया जाता है। बायें को सामान्यतः, तबले की तुलना में निचले स्वरों "मन्द्र पंचम" पर सुर में रखा जाता है। कलाकार अपनी हथेली के पिछले हिस्से (मणिबंध) के दबाव द्वारा भी बायें के सुरों में मामूली बदलाव कर सकते हैं।[२][९]
इन दोनों अंगों के आकार में विषमता के कारण तीखे और चंचल बोल - ता, तिन, ना इत्यादि दाहिने पर बजाये जाते हैं और बायें का आकार बड़ा होने के कारण गंभीर आवाज वाले नाद धे, धिग इत्यादि बायें पर बजते हैं।[३०] इसीलिए "बायें" को "बेस ड्रम" की तरह प्रयोग में लाया जाता है।
तबलों के चमड़ा मढ़े मुख पर भी तीन हिस्से होते हैं:
- चाट, चांटी, किनारा, किनार, की, या स्याही - सबसे किनारे का हिस्सा।
- सुर, मैदान, लव, या लौ - स्याही और किनारे के बीच का भाग।
- बीच, स्याही, सियाही, या गाँव - सबसे बीच का काला हिस्सा, जहाँ एक प्रकार का काला पदार्थ चिपका होता है, जिससे यह हिस्सा मोटा हो जाता है।
तबले के प्रत्येक हिस्से के बीचोबीच एक काले चकत्ते के रूप में जो हिस्सा होता है उसे "स्याही" कहते हैं। यह मुख्य रूप से चावल या गेहूँ के मंड में कई प्रकार की चीजे मिला कर बनाया गया एक लेप होता है जो सूख कर कड़ा हो जाने के बाद तबले के चमड़े की स्वाभाविक धवनि का परिष्कार करके इसे एक खनकदार आवाज़ प्रदान करता है। तबला निर्माण की प्रक्रिया के दौरान स्याही का समुचित प्रयोग एक निपुणता की चीज है और इस वाद्ययंत्र की गुणवत्ता काफ़ी हद तक स्याही आरोपण की कुशलता पर निर्भर होती है।
कुछ वादक, डुग्गी पर सियाही के बजाय, गूँधे गए आटे को चिपका कर सुखा लेते हैं, हालाँकि यह प्रक्रिया हर बार करनी पड़ती है और तबला वादन के बाद इसे खुरच कर हटा दिया जाता है। पंजाब में यह अभी भी प्रचलन में है और ऐसे "बायें" को "धामा" कहते हैं।[४]
तबले के बोल
चित्र:Tabla drums demo.webm तबले के बोलों को "शब्द", "अक्षर" या "वर्ण" भी कहते हैं। ये बोल परंपरागत रूप से लिखे नहीं बल्कि गुरु-शिष्य परम्परा में मौखिक रूप से सीखे सिखाये जाते रहे हैं। इसीलिए इनके नामों में कुछ विविधता देखने को मिलती है। अलग-अलग क्षेत्र और घराने के वादन में भी बोलों का अंतर आता है। एक ही बोल को बजाने के कई तरीकों का प्रचलन भी मिलता है। एक विवरण के अनुसार तबले के मूल बोलों की संख्या पंद्रह है जिनमें से ग्यारह दायें पर बजाये जाते हैं और चार बायें पर।[३१] नीचे डेविड कर्टनी लिखित "फंडामेंटल्स ऑफ़ तबला" और बालकृष्ण गर्ग लिखित बोलों का एक संक्षिप्त और सामान्यीकृत विवरण प्रस्तुत किया गया है[३१]:
- दाहिने के बोल
- ता/ना - किनारा पर तर्जनी (पहली) उउंगली से, ठोकर के बाद उंगली तुरंत उठ जाती है।
- ती - मैदान में तर्जनी से ठोकर, उंगली तुरंत उठ जाती है।
- तिन् - सियाही पर तर्जनी से ठोकर, उंगली तुरंत उठ जाती है।
- ते - तर्जनी अतिरिक्त बाकी तीन उंगलियाँ (या केवल मध्यमा) से सियाही पर, गुंजन नहीं।
- टे - तर्जनी अँगुरी से सियाही पर, गुंजन नहीं।
- तिट - दोहरे ठोकर का बोल, ते और टे का सामूहिक रूप (अन्य उच्चारण तिर)।
- बायाँ के बोल
- धा/धे - पहिली (या दूसरी) उंगली से बीच में ठोकर, मणिबंध (कलाई का पिछला हिस्सा) "मैदान" में रखा रहता है।
- क/के/गे - पूरी हथेली खुली सपाट रख दी जाती है, गुंजन नहीं।
- घिस्सा - बीच में ठोकर के हथेली का पिछला हिस्सा बीच की ओर सरकाया जाता है, जिससे से गुंजन धीरे-धीरे क्रमिक रूप से बंद होता है।
घराने
तबला वादन के कुल छह घराने हैं-
दिल्ली घराने के प्रवर्तक उस्ताद सुधार ख़ाँ थे और पंजाब घराने के अलावा बाकी के चार अन्य घराने भी दिल्ली घराने का ही विस्तार माने जाते हैं। लखनऊ घराने के प्रवर्तक मोदू ख़ाँ और बख़्शू ख़ाँ; फ़र्रूख़ाबाद घराने के प्रवर्तक विलायत अली ख़ाँ उर्फ़ हाजी साहब; अजराड़ा घराने के प्रवर्तक कल्लू ख़ाँ और मीरू ख़ाँ; बनारस घराने के प्रवर्तक पंडित राम सहाय और पंजाब घराने के प्रवर्तक उस्ताद फ़क़ीरबख़्श ख़ाँ थे।[३२]
प्रसिद्ध तबला वादक
प्रसिद्ध तबला वादकों में पंजाब घराने के अल्ला रक्खा ख़ाँ[३३] और ज़ाकिर हुसैन[३४] (पिता पुत्र) का नाम आता है। ज़ाकिर हुसैन को मात्र 37 वर्ष की आयु में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ और वे सबसे कम उम्र में यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति बने, बाद में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ग्रैमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तबला वादन को प्रतिष्ठित कराने में चतुरलाल का उल्लेखनीय योगदान रहा।
बनारस घराने के सामता प्रसाद मिश्र (गुदई महराज), अनोखेलाल मिश्र, कंठे महराज और किशन महाराज (2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित) उल्लेखनीय हैं। इसी घराने के संदीप दास को भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।[३५]
इनके अलावा प्रसिद्ध पाकिस्तानी तबला वादक शौक़त हुसैन ख़ाँ, मुंबई के योगेश शम्सी, त्रिलोक गुर्टू, कुमार बोस, तन्मय बोस, फ़जल क़ुरैशी इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं।
इन्हें भी देखें
टीका-टिप्पणी
| references-column-width
| references-column-count references-column-count-{{#if:1|{{{1}}}}} }}
| {{#if:
| references-column-width }} }}" style="{{#if:
| {{#iferror: {{#ifexpr: 1 > 1 }}
| -moz-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-width: {{#if:1|{{{1}}}}};
| -moz-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; }}
| {{#if:
| -moz-column-width: {{{colwidth}}}; -webkit-column-width: {{{colwidth}}}; column-width: {{{colwidth}}}; }} }} list-style-type: {{#switch: nb
| upper-alpha
| upper-roman
| lower-alpha
| lower-greek
| lower-roman = nb
| #default = decimal}};">
- ↑ In other languages: साँचा:Lang-bn, साँचा:Lang-prs, साँचा:Lang-gu, साँचा:Lang-kn, साँचा:Lang-ml, साँचा:Lang-mr, साँचा:Lang-ne, साँचा:Lang-or, साँचा:Lang-ps, साँचा:Lang-pa, साँचा:Lang-ta, साँचा:Lang-te, साँचा:Lang-ur
सन्दर्भ
| references-column-width
| references-column-count references-column-count-{{#if:1|30em}} }}
| {{#if:
| references-column-width }} }}" style="{{#if: 30em
| {{#iferror: {{#ifexpr: 30em > 1 }}
| -moz-column-width: {{#if:1|30em}}; -webkit-column-width: {{#if:1|30em}}; column-width: {{#if:1|30em}};
| -moz-column-count: {{#if:1|30em}}; -webkit-column-count: {{#if:1|30em}}; column-count: {{#if:1|30em}}; }}
| {{#if:
| -moz-column-width: {{{colwidth}}}; -webkit-column-width: {{{colwidth}}}; column-width: {{{colwidth}}}; }} }} list-style-type: {{#switch:
| upper-alpha
| upper-roman
| lower-alpha
| lower-greek
| lower-roman = {{{group}}}
| #default = decimal}};">
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ २.० २.१ २.२ २.३ Tabla साँचा:Webarchive एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ ४.० ४.१ ४.२ ४.३ साँचा:Cite journal
- ↑ ५.० ५.१ ५.२ ५.३ ५.४ ५.५ साँचा:Cite book
- ↑ ६.० ६.१ ६.२ साँचा:Cite book
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ ९.० ९.१ ९.२ साँचा:Cite book
- ↑ १०.० १०.१ १०.२ १०.३ १०.४ साँचा:Cite book
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ दि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ़ तबला, नेम्पल्ली सदानंद, पॉपुलर प्रकाशन
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ साँचा:Cite book, उद्धरण: "To her left are two girls standing with cymbals in their hands, and two seated playing drums, one with a pair of upright drums like the modern Indian dhol, and the other, sitting cross-legged, with a drum held horizontally, like the modern mirdang."
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ རྫོགས་པ་, तिब्बती अंग्रेजी डिक्शनरी (2011)
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ फ्रांस बल्थाज़र सोल्विन्स, A Collection of Two Hundred and Fifty Coloured Etchings साँचा:Webarchive (1799)
- ↑ web.mit.edu/chintanv/www/tabla/class_material/Introduction%20to%20Tabla.ppt
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ आर॰ स्टीवर्ट, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, UCLA, 1974
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ साँचा:Cite book
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ ३१.० ३१.१ साँचा:Cite book
- ↑ सन्दर्भ त्रुटि: अमान्य
<ref>टैग;Gargनामक संदर्भ की जानकारी नहीं है - ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ संदीप दास को मिला ग्रैमी अवार्ड साँचा:Webarchive, एनडीटीवी पर इंटरव्यू (फ़रवरी 2017)।
आगे पढ़ने हेतु
- दि मेजर ट्रेडिशंस ऑफ़ नॉर्थ इंडियन तबला ड्रमिंग: अ सर्वे प्रेसेंटेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेज बाय इंडियाज लीडिंग आर्टिस्ट्स, लेखक - रॉबर्ट ऍस॰ गौट्लिब, म्युज़िकवर्लाग ई॰ कात्ज़बिश्लर, 1977. ISBN 978-3-87397-300-8. साँचा:En icon
- दि तबला ऑफ़ लखनऊ: अ कल्चरल ऍनालिसिस ऑफ़ अ म्यूज़िकल ट्रेडिशन, लेखक - जेम्स किपेन, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1988. ISBN 0-521-33528-0. साँचा:En icon
- सोलो तबला ड्रमिंग ऑफ़ नॉर्थ इंडिया: टेक्स्ट & कमेंटरी, लेखक - रॉबर्ट ऍस॰ गौट्लिब, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, 1993. ISBN 81-208-1093-7. साँचा:En icon
- फंडामेंटल्स ऑफ़ तबला, (भाग 1). लेखक - डेविड आर॰ कर्टनी, सुर संगीत सर्विसेस प्रकाशन, 1995. ISBN 0-9634447-6-X. साँचा:En icon
- एडवांस्ड थ्योरी ऑफ़ तबला, (भाग 2). लेखक - डेविड आर॰ कर्टनी, सुर संगीत सर्विसेस प्रकाशन, 2000. ISBN 0-9634447-9-4. साँचा:En icon
- मैन्युफैक्चर एंड रिपेयर ऑफ़ तबला, (भाग 3). लेखक - डेविड आर॰ कर्टनी, सुर संगीत सर्विसेस प्रकाशन, 2001. ISBN 1-893644-02-2. साँचा:En icon
- फोकस ऑन कायदाज ऑफ़ तबला, (भाग 4). लेखक - डेविड आर॰ कर्टनी, सुर संगीत सर्विसेस प्रकाशन, 2002. ISBN 1-893644-03-0. साँचा:En icon
- थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ़ तबला, लेखक- सदानंद नाइमपल्ली, पॉपुलर प्रकाशन, 2005. ISBN 81-7991-149-7 साँचा:En icon
बाहरी कड़ियाँ
- ऍसऍसबी रेडियो, ऑस्ट्रेलिया - प्रसारण: बनारस घराने के पंडित चन्द्रनाथ शास्त्री का इंटरव्यू, बनारस घराने की विशिष्टताओं पर। साँचा:En icon